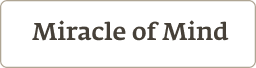क्या नदियों को जोड़ने से पानी की समस्या सुलझेगी?
एक तरफ़ नदियों का घटता जल-स्तर तो दूसरी तरफ़ बाढ़ जैसी विपदाओं से जूझते देश के लिए क्या नदियों को आपस में जोड़ने की योजना कारगर होगी? इस योजना की क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं?
प्रश्न: सद्गुरु, क्या आप रिवर-इंटरलिंकिंग (नदी जोड़) और जल-यातायात बढ़ाने के प्रस्ताव से सहमत हैं? क्या ये चीज़ें आने वाले समय में लाभदायक होंगी या उनसे हानि हो सकती है?
सद्गुरु: जब भी हम पानी के रि-डिस्ट्रिब्यूशन (दोबारा बंटवारे) पर विचार करें तो इसे बहुत सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। हो सकता है कहीं बाढ़ रोकने के लिए ऐसा करना जरुरी हो। पर अगर आपको लगता है कि नदियों को जोड़ने से समस्याओं का अंत हो जाएगा तो ऐसा सोचना गलत है।
Subscribe
उदाहरण के लिए, पिछले कुछ दशकों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में मानूसन कमज़ोर हो रहा है। कई इलाक़ों में वर्षा की अब बहुत कम दिनों के लिए और अकसर तेज़ होती है। इन बदलावों के कारण उन “अधिक पानी” वाली नदियों को भी जल की कमी का संकट झेलना पड़ सकता है।
समाधान का मूल्यांकन
कुछ इंटरलिंक करने वाले प्रोजेक्ट आरंभ किए गए हैं। अगर हम नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले इनसे होने वाले आर्थिक लाभों और प्राकृतिक संसाधनों को होने वाली हानि का विश्लेषण कर लें तो बेहतर होगा। कुछ नदियों को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना बाढ़ को रोकने में मददगार होगा। पर भारत की सभी नदियों को इस काम के लिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि हमारी नदियाँ यूरोपियन या उत्तरी अमेरिका की नदियों की तरह नहीं हैं। मिसाल के लिए यूरोप में एक साल में औसत पतन 100 से 150 दिन तक होता है। और दो से तीन माह तक दस से पंद्रह इंच तक बर्फ की तह जमी रहती है। हमारे यहाँ पतन साल में 60-70 दिन तक होता है, और यहाँ ऊष्ण-कटिबंधिय इलाक़े हैं, जहाँ जमीन जल्दी से सारा पानी सोख लेती है।
प्रश्न: पिछले सालों में नदियों के कुदरती बहाव में कमी आई है क्योंकि पानी की भारी मात्रा नहरों के ज़रिए कृषि व उद्योग में चली जाती है। आपका इस बारे में क्या विचार है?
सद्गुरु: भारत में कृषि नदियों का साठ से अस्सी प्रतिशत जल ले रही है। अगर हम ऐसी फसलें उगाने वाले दूसरे देशों को देखें तो वे कम पानी का इस्तेमाल करते हुए, बेहतर पैदावार उगा रहे हैं। हमारी नीति की सिफारिश में यही सलाह दी गई है कि वृक्षों पर आधारित कृषि को अपनाई जाए जिसमें माईक्रो-सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। अगर हमने सही तरह की तकनीकों को अपनाया और धरती पर अनिवार्य ह्यूमस (खाद-मिट्टी) पैदा कर सके तो पानी की खपत घटेगी और इसी से नदी का प्रवाह भी बना रहेगा।
हमें यह समझना होगा कि बड़े बांध तब बने, जब हम एक देश के तौर पर स्वयं को बचाने की चुनौती से जूझ रहे थे । 1947 में हम एक ऐसे देश की तरह थे जिसके पास जीने के पर्याप्त साधन नहीं थे। औसत जीवन काल महज़ बत्तीस वर्ष था। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार नहीं था - अंग्रेजों के जाने के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था।
उत्तरजीविता से वहनीयता की ओर
लगभग पचास सालों में, हमने उत्तरजीविता के लिहाज से बहुत कुछ किया है। एक देश के जीवन में ऐसा होता है। बदकिस्मती से हमारी जनसंख्या तेजी से कई गुना बढ़ी - ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रजनन के कारण ऐसा हुआ - लोगों का संभावित जीवन काल बढ़ा, जो एक अच्छी उपलब्धि रही। लेकिन हम तैंतीस करोड़ से एक सौ तीस करोड़ पर आ गए। इस तरह धरती पर दबाव बढ़ा है। धरती पर जनसंख्या का अनुपात भारत में बहुत बुरा है। हमें इन्हीं सभी हकीकतों के साथ काम करना होगा। तो पहले पचास सालों तक हम ‘सरवाइवल मोड’ (जीवित रहने के लिए काम) में रहे, पिछले बीस सालों से हम ‘डेवलपमेंट मोड’ (विकास के लिए काम) में हैं । अब समय आ गया है - ‘रैली फार रिवर्स’ एक नया मोड़ है - जहाँ से हमें खुद को ‘सस्टेनेबल मोड’ (कायम रहने वाले तरीकों को अपनाना) में लाना होगा।